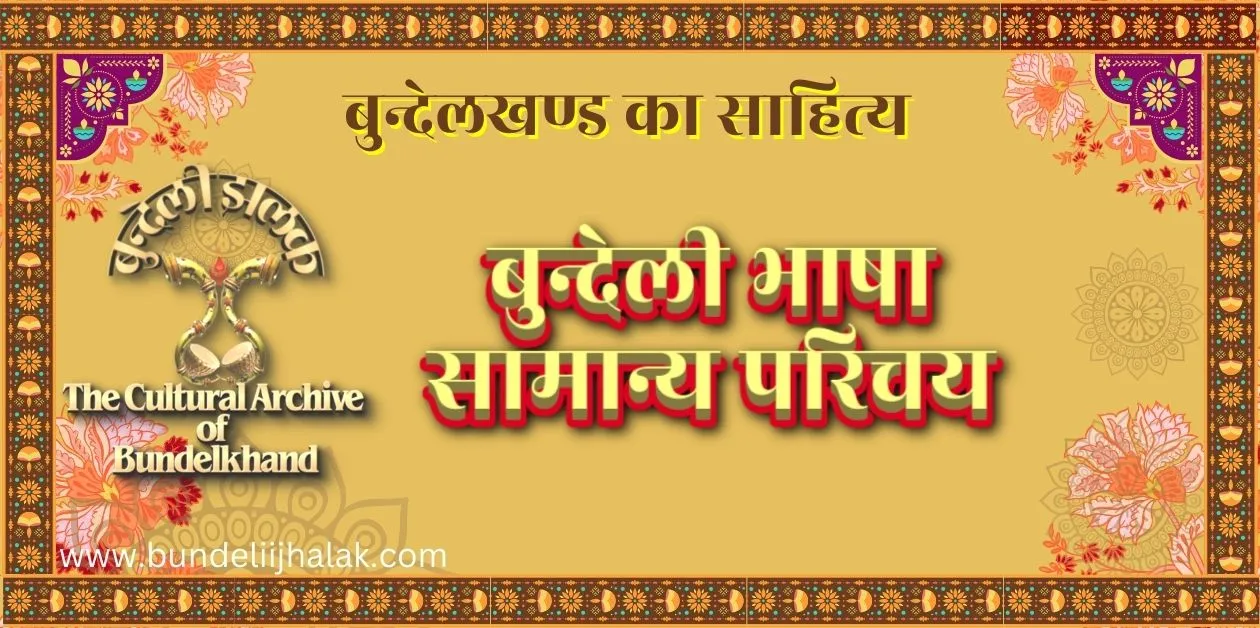‘बुन्देली-भाषा’ Bundeli Bhashaके साहित्य का उद्भव लगभग बारहवीं शताब्दी ईसवी से माना जाता है। क्योंकि ‘आल्हा-खण्ड’ की रचना मूलतः बुन्देली में हुई, कालान्तर में स्थानीयता के कारण उसमें बुन्देली और बघेली लोकभाषा का मिश्रण हो गया, जिसे ग्रियर्सन ने ‘बनाफरी’ बोली नाम दिया है। आल्हा-खण्ड के रचयिता जगनिक महोबा के चन्देल राजा परमर्दिदेव समय के आश्रित कवि थे।
इसके बाद गोस्वामी विष्णुदास (महाभारत- कथा), मानिककवि (वैताल-पच्चीसी), मेघनाथ (भगवतगीता – भाषा) ये सभी उस समय की व्यापक काव्य- भाषा ‘ग्वालियरी’ के कवि माने जाते हैं। बुन्देली -भाषा एवं साहित्य के विकास में- बुन्देला शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओरछा- राज्य के महाराजा भारतीचन्द के दरबारी कवियों में मनसाराम सिद्ध (गुप्तभेद), खेमराज (प्रताप हजारा) और आचार्य कृपाराम (हिततरंगिनी) प्रसिद्ध काव्यकार थे।
महाराजा मधुकरशाह (1554 से 1 592 ई.) स्वयं कवि थे तथा कृष्ण भक्त कवियों के आश्रयदाता थे। उनके समय में हरीराम व्यास (रागमाला) व मोहनदास मिश्र (रामाश्वमेघ) प्रसिद्ध कवि थे। बुन्देली काव्य-परम्परा का चरमोत्कर्ष आचार्य केशवदास की काव्य रचना से होता है। महाराज इन्द्रजीत सिंह के आश्रय में केशवदास को राजगुरू और राजकवि की प्रतिष्ठा मिली।
उनकी शिष्या प्रवीणराय इन्द्रजीत सिंह की सभा की प्रसिद्ध नर्तकी एवं भावपूर्ण कवियित्री थी। अपने एक अन्य आश्रयदाता ‘ ओरछेश वीरसिंह देव प्रथम (1605 से 1627 ई ) के दरबार में रहकर आचार्य केशवदास ने रामचन्द्रिका, रसिक- प्रिया , कविप्रिया, वीरसिंह -चरित्र आदि प्रसिद्ध कृतियों की रचना की।
दतिया-राज्य अपनी स्थापना काल में ही कवि, पंडितों, कलाकारों के आश्रय का केन्द्र था। दतिया के राजा रामचन्द्र राव (1707 से 1734 ई) साहित्यिक – अभिरुचि के व्यक्ति थे। उनके दरबार में खण्डन-कवि (सुदामा समाज) , केस कवि (माधवानल) नाटक तथा जोगीदास (दलपतराव -रासो) आश्रित कवि मौजूद थे। अक्षर अनन्य का जन्म यद्यपि ओरछा में हुआ था लेकिन वे दतिया के राजाओं के अश्रित कवि रहे अष्ठांग-योग उनकी ठेठ बुन्देली रचना मानी जाती है।
बुन्देली भाषा व साहित्य के उत्थान में ओरछा व दतिया के साथ पन्ना-केन्द्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। पन्ना-नरेश वीर छत्रसाल अस्त्र-शस्त्र के साथ लेखनी के भी धनी थे। वे अलौकिक भावुकता से युक्त उच्चकोटि के कवि थे। प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि ने उनकी कविताओं के संग्रह को ‘छत्नसाल ग्रन्थावलि’ के नाम से सम्पादन किया है। महाराज छत्रसाल के दरबारी राजाश्रित कवि गोरेलाल लाल कवि ने ‘छत्रप्रकाश’ तथा भूषण ने ‘छत्रसाल-दसक’ काव्य की रचना की थी।
बुन्देली भाषा के विकास में छत्रसाल के गुरू प्राणनाथ विरचित ‘प्रणाली-साहित्य‘ का भी उल्लेखनीय योगदान रहा, जिसमें प्रानाथ के दो शिष्यों, लालदास व मुकुन्ददास की काव्य-रचनाएं भी शामिल हैं। पन्ना दरबार के आश्रित कवियों में बोधा-कवि (विरह नवारीश) तथा बख्शी हंसराज उर्फ प्रेम सखि (स्नेहसागर| का नाम भी आता है।
उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में बुन्देली भाषा में बांदा के पदुमाकर भट्ट ओरछा के ठाकुर-कवि और पन्ना के पजनेश मूलतः श्रंगार-रस के कवि थे। इन्हीं के साथ ईसुरी , गंगाधर व्यास व ख्याली राम की रची फागें बुन्देलखण्ड में प्रचलित हैं।
बीसवीं सदी के बुन्देली भाषा के कवियों में रामचरण हयारण मित्र‘, डॉ दुर्गेश दीक्षित, पण्डित गुणसागर सत्यार्थी, पद्मश्री अवध किशोर जड़िया आदि कई नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार बुन्देली भाषा के विकास के साथ-साथ उसके साहित्य की समंद्ध परम्परा प्राप्त होती है।
जब से बुन्देलखण्ड में बुन्देलों का शासन आरम्भ हुआ, बुन्देली ही उनकी राजभाषा रही। बुन्देला शासकों का राज्य-कार्य , हिसाब-किताब और परस्पर का पत्र-व्यवहार सभी बुन्देली भाषा में सम्पन्न होता रहा। शिष्ट साहित्य के साथ-साथ जनसामान्य में पर्याप्त लोकसाहित्य का भी सृजन हुआ, जो अनेक प्रकार के गीतों, कथाओं, लोकोक्तियों गाथाओं व लोकनाट्यों आदि के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, जिनमें लोक-भाषा के रूप में बुन्देली की समृद्ध परम्परा मिलती है।
‘बुन्देली-भाषा’ के साहित्य का उद्भव लगभग बारहवीं शताब्दी ईसवी से माना जाता है। क्योंकि ‘आल्हा-खण्ड’ की रचना मूलतः बुन्देली में हुई, कालान्तर में स्थानीयता के कारण उसमें बुन्देली और बघेली लोकभाषा का मिश्रण हो गया, जिसे ग्रियर्सन ने ‘बनाफरी’ बोली नाम दिया है। आल्हा-खण्ड के रचयिता जगनिक महोबा के चन्देल राजा परमर्दिदेव समय के आश्रित कवि थे।
इसके बाद गोस्वामी विष्णुदास (महाभारत- कथा), मानिककवि (वैताल-पच्चीसी), मेघनाथ (भगवतगीता – भाषा) ये सभी उस समय की व्यापक काव्य- भाषा ‘ग्वालियरी’ के कवि माने जाते हैं।
बुन्देली -भाषा एवं साहित्य के विकास में बुन्देला शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओरछा- राज्य के महाराजा भारतीचन्द के दरबारी कवियों में मनसाराम सिद्ध (गुप्तभेद) , खेमराज (प्रताप हजारा) और आचार्य कृपाराम (हिततरंगिनी) प्रसिद्ध काव्यकार थे।
महाराजा मधुकरशाह (1554 से 1 592 ई.) स्वयं कवि थे तथा कृष्ण भक्त कवियों के आश्रयदाता थे। उनके समय में हरीराम व्यास (रागमाला) व मोहनदास मिश्र (रामाश्वमेघ) प्रसिद्ध कवि थे। बुन्देली काव्य-परम्परा का चरमोत्कर्ष आचार्य केशवदास की काव्य रचना से होता है। महाराज इन्द्रजीत सिंह के आश्रय में केशवदास को राजगुरू और राजकवि की प्रतिष्ठा मिली।
उनकी शिष्या प्रवीणराय इन्द्रजीत सिंह की सभा की प्रसिद्ध नर्तकी एवं भावपूर्ण कवियित्री थी। अपने एक अन्य आश्रयदाता ‘ ओरछेश वीरसिंह देव प्रथम (1605 से 1627 ई ) के दरबार में रहकर आचार्य केशवदास ने रामचन्द्रिका, रसिक- प्रिया , कविप्रिया, वीरसिंह -चरित्र आदि प्रसिद्ध कृतियों की रचना की।
दतिया-राज्य अपनी स्थापना काल में ही कवि, पंडितों, कलाकारों के आश्रय का केन्द्र था। दतिया के राजा रामचन्द्र राव (1707 से 1734 ई) साहित्यिक – अभिरुचि के व्यक्ति थे। उनके दरबार में खण्डन-कवि (सुदामा समाज) , केस कवि (माधवानल) नाटक तथा जोगीदास (दलपतराव -रासो) आश्रित कवि मौजूद थे। अक्षर अनन्य का जन्म यद्यपि ओरछा में हुआ था लेकिन वे दतिया के राजाओं के अश्रित कवि रहे अष्ठांग-योग उनकी ठेठ बुन्देली रचना मानी जाती है।
बुन्देली भाषा व साहित्य के उत्थान में ओरछा व दतिया के साथ पन्ना-केन्द्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। पन्ना-नरेश वीर छत्रसाल अस्त्र-शस्त्र के साथ लेखनी के भी धनी थे। वे अलौकिक भावुकता से युक्त उच्चकोटि के कवि थे। प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि ने उनकी कविताओं के संग्रह को ‘छत्नसाल ग्रन्थावलि’ के नाम से सम्पादन किया है। महाराज छत्रसाल के दरबारी राजाश्रित कवि गोरेलाल लाल कवि ने ‘छत्रप्रकाश’ तथा भूषण ने ‘छत्रसाल-दसक’ काव्य की रचना की थी।
बुन्देली भाषा के विकास में छत्रसाल के गुरू प्राणनाथ विरचित ‘प्रणाली-साहित्य‘ का भी उल्लेखनीय योगदान रहा, जिसमें प्रानाथ के दो शिष्यों, लालदास व मुकुन्ददास की काव्य-रचनाएं भी शामिल हैं। पन्ना दरबार के आश्रित कवियों में बोधा-कवि (विरह नवारीश) तथा बख्शी हंसराज उर्फ प्रेम सखि (स्नेहसागर| का नाम भी आता है।
उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में बुन्देली भाषा में बांदा के पदुमाकर भट्ट ओरछा के ठाकुर-कवि और पन्ना के पजनेश मूलतः श्रंगार-रस के कवि थे। इन्हीं के साथ ईसुरी , गंगाधर व्यास व ख्याली राम की रची फागें बुन्देलखण्ड में प्रचलित हैं।
बीसवीं सदी के बुन्देली भाषा के कवियों में रामचरण हयारण मित्र‘, डॉ दुर्गेश दीक्षित, पण्डित गुणसागर सत्यार्थी, पद्मश्री अवध किशोर जड़िया आदि कई नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार बुन्देली भाषा के विकास के साथ-साथ उसके साहित्य की समंद्ध परम्परा प्राप्त होती है।
जब से बुन्देलखण्ड में बुन्देलों का शासन आरम्भ हुआ, बुन्देली ही उनकी राजभाषा रही। बुन्देला शासकों का राज्य-कार्य , हिसाब-किताब और परस्पर का पत्र-व्यवहार सभी बुन्देली भाषा में सम्पन्न होता रहा। शिष्ट साहित्य के साथ-साथ जनसामान्य में पर्याप्त लोकसाहित्य का भी सृजन हुआ, जो अनेक प्रकार के गीतों, कथाओं, लोकोक्तियों गाथाओं व लोकनाट्यों आदि के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, जिनमें लोक-भाषा के रूप में बुन्देली की समृद्ध परम्परा मिलती है।
According to the National Education Policy 2020, it is very useful for the Masters of Hindi (M.A. Hindi) course and research students of Bundelkhand University Jhansi’s university campus and affiliated colleges.